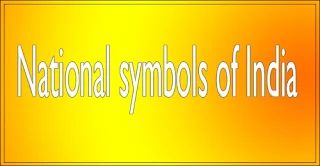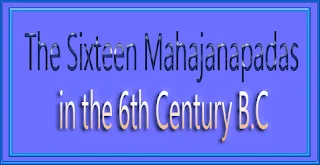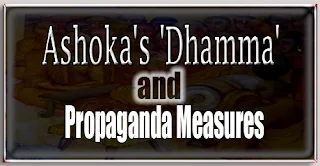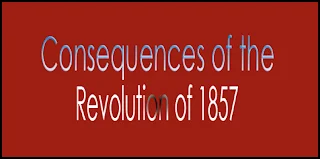| क्र० | नाम | पद अवधि |
| 1. | सुकुमार सेन | 21 मार्च, 1950 - 19 दिसम्बर, 1958 |
| 2. | के०वी०के० सुंदरम | 20 दिसम्बर, 1958 - 30 सितम्बर, 1967 |
| 3. | एस०पी० सेन वर्मा | 1 अक्टूबर, 1967 - 30 सितम्बर, 1972 |
| 4. | डॉ० नगेन्द्र सिंह | 1 अक्टूबर, 1972 - 6 फरवरी, 1973 |
| 5. | टी० स्वामीनाथन | 7 फरवरी, 1973 - 17 जून, 1977 |
| 6. | एस०एल० शकधर | 18 जून, 1977 - 17 जून, 1982 |
| 7. | आर०के० त्रिवेदी | 18 जून, 1982 - 31 दिसम्बर, 1985 |
| 8. | आर०वी०एस० पेरिशास्त्री | 1 जनवरी, 1986 - 25 नवम्बर, 1990 |
| 9. | श्रीमती वी०एस० रमादेवी | 26 नवम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1990 |
| 10. | टी०एन० शेषन | 12 दिसम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1996 |
| 11. | एम०एस० गिल | 12 दिसम्बर, 1996 - 13 जून, 2001 |
| 12. | जे०एम० लिंगदोह | 14 जून, 2001 - 7 फरवरी, 2004 |
| 13. | टी०एस० कृष्णामूर्ति | 8 फरवरी, 2004 - 15 मई, 2005 |
| 14. | बी०बी० टंडन | 16 मई, 2005 - 29 जून, 2006 |
| 15. | एन० गोपालस्वामी | 30 जून, 2006 - 20 अप्रैल, 2009 |
| 16. | नवीन चावला | 21 अप्रैल, 2009 - 29 जुलाई, 2010 |
| 17. | एस०वाई० कुरैशी | 30 जुलाई, 2010 - 10 जून, 2012 |
| 18. | वी०एस० संपत | 11 जून, 2012 - 15 जनवरी, 2015 |
| 19. | हरिशंकर ब्रह्मा | 16 जनवरी, 2015 - 18 अप्रैल, 2015 |
| 20. | नसीम जैदी | 19 अप्रैल, 2015 - 5 जुलाई, 2017 |
| 21. | अचल कुमार ज्योति | 6 जुलाई, 2017 - 22 जनवरी, 2018 |
| 22. | ओम प्रकाश रावत | 23 जनवरी, 2018 - 1 दिसम्बर, 2018 |
| 23. | सुनील अरोड़ा | 2 दिसम्बर, 2018 - 12 अप्रैल, 2021 |
| 24. | सुशील चन्द्रा | 13 अप्रैल, 2021 - 14 मई, 2022 |
| 25. | राजीव कुमार | 15 मई, 2022 - 18 फरवरी, 2025 |
| 26. | ज्ञानेश कुमार | 19 फरवरी, 2025 - अब तक |
 |
| Chief Election Commissioner of India |