अशोक भारतीय इतिहास में न सिर्फ विजेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में विख्यात है, बल्कि वह स्वयं अपने जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रयत्नशील था। कलिंग युद्ध के पश्चात उसने मानव कल्याण की तरफ ध्यान दिया। अशोक ने जिस धार्मिक विचार का प्रतिपादन किया, वह 'धम्म' (Dhamma) के नाम से जाना जाता है। उसके प्रचार एवं प्रसार के लिए अशोक ने अनेक उपाय किए।
धम्म का स्वरूप (Nature of Dhamma ) : अशोक के धम्म का स्वरूप विद्वानों के बीच एक मतभेद का विषय है। इस सम्बन्ध में मुख्यतः दो धारणाएं - कुछ विद्वान इसे बौद्ध धर्म मानते हैं तो कुछ दूसरे विद्वान इसे अशोक की खोज मानते हैं। कुछ विद्वान उसे जैन धर्मावलम्बी भी मानते हैं। डॉ० आर० सी० भंडारकर के मत में अशोक का 'धम्म' धर्मनिरपेक्ष बौद्ध धर्म था। कुछ विद्वान अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म का ही परिवर्तित स्वरूप मानते हैं।
परन्तु बौद्ध धर्म से समानता रहने के बावजूद अशोक के 'धम्म' में बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा नहीं की गयी है। इसमें "चार आर्य सत्य" अष्टांगिक मार्ग या निर्वाण का उल्लेख नहीं मिला है। अशोक न तो अपने धम्म के लिए संघ की व्यवस्था करता है और न ही भिक्षुक का जीवन व्यतीत करने को कहता है। अतः अनेक समानताओं के बावजूद अशोक का 'धम्म' बौद्ध धर्म से भिन्न है। इसलिए अनेक विद्वानों का विचार है कि अशोक का 'धम्म' किस
खास सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्धित नहीं था बल्कि वह सभी भारतीय धर्मा के लिए समान था।
इस प्रकार अशोक के धम्म की तुलना अकबर के दीन-ए-इलाही से कर सकते हैं। अशोक ने सभी धर्मों में प्रचलित बातों को अपना लिया एवं मानव कल्याण के लिए उसका प्रचार किया। इस अर्थ में अशोक का 'धम्म' कोई धर्म न होकर मानव के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने वाला रास्ता था, यह वह मार्ग था जिसका पालन करने से मानव को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती थी। अशोक के धम्म की पृष्ठभूमि : यद्यपि व्यक्तिगत तौर पर अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, परन्तु जनता के लिए उसने अपने धम्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का नहीं। इस धम्म की स्थापना के पीछे कई कारण थे
अशोक की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण यह था कि हिन्दू धर्म की कुरीतियों के चलते जैन एवं बौद्ध धर्म का अच्छा प्रसार हो चुका था। ये धर्म वैदिक धर्म से कम कठोर थे, अतः जनता में उनका अच्छा प्रभाव था। धार्मिक आन्दोलनों ने सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया था। ऐसी स्थिति में टकराव की सम्भावना थी। इसको रोकने तथा सामाजिक एकता बनाये रखने के लिए तथा जनसाधारण की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ही अशोक ने 'धम्म' का आविष्कार किया। इसके बहुत व्यावहारिक लाभ थे।
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी 'धम्म' आवश्यक था। अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य का काफी विस्तार हो चुका था। इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न जातियाँ एवं राजनीतिक इकाइयाँ थी। इन सभी को बाँध कर रखना एक कठिन कार्य था। इन सब कारणों के चलते अशोक ने 'धम्म' का आविष्कार किया एवं इसके प्रचार के लिए अनेक उपाए किए। अपने 'धम्म' का आधार उसने बौद्ध धर्म को इसलिए बनाया क्योंकि उस समय यह सबसे अधिक प्रचलित था एवं इसमें जटिलता नहीं थी।
धम्म के प्रचार के उपाय : अशोक एक सिद्धान्तवादी की तरह सिर्फ 'धम्म' की व्याख्या करके चुप नहीं बैठ गया बल्कि धम्म प्रचार के लिए उसने अनेक उपाय किये।
अपने धर्म के प्रचार के सन्दर्भ में अशोक ने प्रधान स्थान धर्म श्रवण को दिया। यह घोषणा राजकर्मचारियों एवं जनसाधारण दोनों के मध्य करवायी गयी। इसके लिए पुरूषों एवं राजुकों को आवश्यक निर्देश दिए गए। तृतीय शिलालेख में अशोक ने यह आज्ञा भी दी कि उसके साम्राज्य में सर्वत्र मुक्त, राजुक और प्रादेशिक पाँच-पाँच वर्षो पर धर्मानुशासन के लिए निकलें। इस धर्मानुशासन के लिए अशोक ने दो उपाए किए-धर्म स्तंभों की स्थापना एवं धर्म महामात्रों की नियुक्ति |
अशोक ने विभिन्न स्थानों पर (प्रमुख मार्गो पर शिलाओं के स्तम्भ पर अपने विचारों को लिपिबद्ध करवाया जिससे जनसाधारण अशोक के विचारों को जान सके और उनका पालन कर सके। अशोक के अभिलेखों की संख्या काफी बड़ी है। इनसे अशोक के धार्मिक विचारों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन अभिलेखों के खुदवाने का यह भी उद्देश्य था कि ये चिरस्थायी हो और उसके उत्तराधिकारी इनका अनुसरण कर सके।
धम्म प्रचार के लिए अशोक ने एक मौलिंक कार्य किया। यह था धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अपने राज्याभिषेक के 13 वे वर्ष में अशोक ने इन्हें नियुक्त किया। धार्मिक क्षेत्र में इनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। इतना ही नहीं, अशोक ने व्यक्तिगत जीवन को भी धर्मानुकूल बना लिया। उसने मांस-मदिरा का त्याग कर दिया। महल में पशु-वच कम करवा दिया, दान और सार्वजनिक हित के लिए काम किया। हिसापूर्ण समारोहों को बन्द करवा दिया तथा धार्मिक आयोजन एवं समारोह मनाना प्रारंभ किया। विविध प्रदर्शनों में भी धर्म की वृद्धि हुई। इन प्रदर्शनों में विमान दर्शन, हस्तिदर्शन, अग्निकन्ध एवं अन्य, "दिव्य रूप" के दर्शन कराए जाते थे। अशोक ने धर्म यात्रा प्रारम्भ की। अशोक ने अपने साम्राज्य के बाहर भी धर्म का प्रचार किया। उसके अभिलेखों में दक्षिण के राज्यों एवं विदेशी शासकों का उल्लेख मिलता है जहाँ अशोक ने धर्म प्रचार हेतु अपने दूत भेजे। साथ-ही-साथ अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी प्रयत्न किये। उसी समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा हुई जिसमें महेन्द्र एवं संघमित्रा (अशोक के पुत्र-पुत्री) को श्रीलंका में प्रचार के लिये भेजा गया। प्रो० योगेन्द्र मिश्र का कहना है कि अशोक के प्रचार ने बौद्ध-धर्म को विश्वधर्म में परिवर्तित कर दिया। यद्यपि अशोक का धर्म (धम्म) बौद्ध नहीं था, फिर भी उसके प्रचारक जब बाहर गये होंगे तब बाहर वालों ने उन्हें बौद्ध ही समझा होगा। फलतः यहूदी धर्म और ईसाई धर्म पर बौद्ध धर्म का जो प्रभाव पड़ा उसका श्रेय कुछ अंशी में अशोक को दिया जा सकता है।
अशोक ने इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने मानवोचित गुणों के विकास के पालन पर जोर दिया जिससे मानव कल्याण हो सके। अशोक के धर्म की अपनी विशिष्टता है। वह जीवन के व्यवहारिक पहलू पर जोर देता था, नागरिकों में सामाजिक नैतिकता का विकास करना चाहता था।
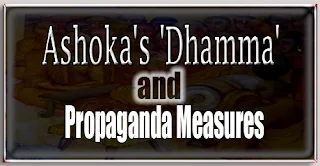 |
| Ashoka's 'Dhamma' and Propaganda Measures |
End of Articles.... Thanks.....

No comments:
Post a Comment