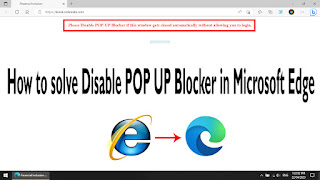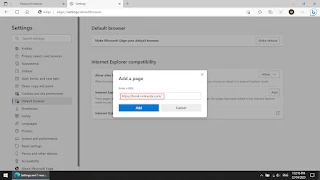Friday, 10 March 2023
Wednesday, 8 February 2023
Thursday, 26 January 2023
Full Forms of Computer Words starting with - A
A/D : Analog to digitalAI : Artificial intelligence
ALGOL : Algorithmic Language
ALU : Arithmetic Logic Unit
AM : Amplitude Modulation
AMD : Advanced Micro Devices
ANSI : American National standards Institute
ARP : Address resolution Protocol
Full Forms of Computer Words starting with - B
Full Forms of Computer Words starting with -C
Full Forms of Computer Words starting with -D
Full Forms of Computer Words starting with -E
Full Forms of Computer Words starting with -F
Full Forms of Computer Words starting with -G
Full Forms of Computer Words starting with -H
Full Forms of Computer Words starting with -I
Full Forms of Computer Words starting with -J
Full Forms of Computer Words starting with -K
Full Forms of Computer Words starting with -L
Full Forms of Computer Words starting with -M
Full Forms of Computer Words starting with -N
Full Forms of Computer Words starting with -O
Thursday, 15 December 2022
 |
| The Achievements of Louis XIV |
Friday, 18 November 2022
नानकिंग की संधि
29 अगस्त, 1842 को चीन और ब्रिटेन में समझौता हो गया। यह समझौता नानकिंग को सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं-
(क) ब्रिटिश व्यापारियों के लिए चीन के पाँच वन्दरगाह कैंटन (Canton ), अमॉय (Amoy) फूलों (Phoolon), निंगपो (Ningpo) एवं संघाई (Shanghai) खोल दिये गये जहाँ ब्रिटिश सरकार को वाणिज्यदूत नियुक्त करने का अधिकार मिल गया।
(ख) हांगकांग का द्वीप सदा के लिए अंग्रेजों को मिल गया।
(ग) विदेशी व्यापार का नियंत्रण करने वाले चीनी व्यापारियों के संगठन को हांग को भंग कर दिया गया ताकि ब्रिटिश व्यापारियों को चीनी व्यापारियों से सीधे क्रय-विक्रय का अधिकार दे दिया गया। (घ) चीन में आयात-निर्यात के सीमा शुल्क की दरें निश्चित कर दी गई। पाँच प्रतिशत (मूल्यानुसार) तट कर निर्धारित किया गया।
(ड़) चीन ने दो करोड़ दस लाख डालर देना मान लिया। इसमें साठ लाख डालर तो कँटन में अफीम जब्त करने के बदले क्षतिपूर्ति, तीस जाख डालर हाँग व्यापारियों के पास बकाया तथा एक करोड़ बीस लाख डालर युद्ध क्षतिपूर्ति थी।
(च) यह प्रबंध मान लिया गया कि मुख्य ब्रिटिश प्रतिनिधि और चीनी अधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार को 'प्रार्थना-पत्र' न कहकर 'सन्देश पत्र' कहा जाएगा।
(छ) यह मान लिया गया कि अंग्रेजों पर मुकदमें उन्हीं के कानून के अनुसार और उन्हीं की अदालत में चलेंगे।
(ज) यह भी निश्चय हुआ कि जो सुविधाएँ अन्य विदेशियों को दी जाएगी, वे सुविधाएँ इन्हें भी दी जाएगी।
नानकिंग की सौंध चीन के लिए अत्यंत अपमानजनक साबित हुई। इसने मंचू सरकार की कमजोरी स्पष्ट कर दी। यह भी स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध आसान नहीं है। जिस अफीम व्यापार को बंद करने के लिए युद्ध किया गया था, वह ज्यों का त्यों बना रहा। प्रसंगवश, मंच सरकार ने हारकर ब्रिटेन से नानकिंग की संधि को इस संधि में 13 धाराएँ थीं। यह संधि चीन द्वारा विदेशी हमलावरों के साथ संपन्न की गई पहली असमान संधि थी। इस सौंध में मुख्यतया यह निर्धारित किया गया कि क्वांगचो, फूचओ, श्यामन, निंगपो और शंधाई-इन पाँचों शहरों को ब्रिटेन के व्यापार के लिए खोल दिया जाएगा; हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया जाएगा और चीन ब्रिटेन को 2 करोड़ 10 लाख चाँदी के डालर (सिक्के) हजाने के तौर पर देगा। इसमें यह व्यवस्था भी थी कि ब्रिटिश माल के प्रवेश पर लगनेवाला सीमा शुल्क दोनों देशों की बातचीत के जरिए निर्धारित किया जाएगा।
1843 ई० में ब्रिटेन ने मंचू सरकार को मजबूर कर नानकिंग सौंध के पूरक दस्तावेजों चीन के पाँच शहरों में ब्रिटेन के व्यापार से संबद्ध सामान्य नियमावली' और 'चीन ब्रिटेन हमन संधि' पर भी हस्ताक्षर करवा लिए। इन दोनों दस्तावेजों में यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटेन का जो भी माल चीन में आयात किया जाएगा या चीन से बाहर भेजा जाएगा उसपर 5 प्रतिशत से ज्यादा सीमा शुल्क नहीं लगेगा, तथा संधि में निर्धारित पाँच शहरों में अंगरेजों को अपनी बस्तियाँ बसाने के लिए पट्टे पर जमीन लेने की इजाजत होगी। (इस व्यवस्था से चीन में विदेशियों के लिए पट्टे पर भूमि लेने' और उसपर विदेशी बस्तियाँ बसाने का रास्ता खुल गया। इसके अलावा ब्रिटेन ने चीन की धरती पर विदेशी कानून लागू करने और 'विशेष सुविधाप्राप्त राष्ट्र का वर्ताव' पाने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया।
1844 ई० में अमेरिका और फ्रांस ने मंचू सरकार को क्रमशः 'चीन-अमेरिका वांगश्या साँध' और 'चीन-फ्रांस व्हांगफू संधि पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। इन दो संधियों के जरिए अमेरिका और फ्रांस ने चीन से प्रादेशिक भूमि व हर्जाने को छोड़कर बाकी सभी ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए जिनकी चर्चा नानकिंग सोध एवं उससे संबद्ध दस्तावेजों में की गई थी। इसके अलावा, अमेरिकियों ने अपने देश के व्यापार के सुरक्षा के लिए चीनी व्यापारिक बंदरगाहों में युद्धपोत भेजने और पाँच व्यापारिक बंदरगाह शहरों में चर्च एवं अस्पताल बनाने के विशेषाधिकार भी प्राप्त कर लिए। इसी दौरान फ्रांसीसी भी मंचू सरकार को इस बात के लिए मजबूर करने में सफल हो गए कि वह व्यापारिक बंदरगाहों में रोमन कैथोलिकों की गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध उठा लें, ताकि वे अपने इच्छानुसार धर्म प्रचार कर सकें। जल्दी ही प्रोटेस्टेंट मिशनरियों ने भी यह अधिकार प्राप्त कर लिया।
नानकिंग की संधि और दूसरी असमान संधियों पर हस्ताक्षर होने के फलस्वरूप चीन एक प्रभुसत्ता संपन्न देश नहीं रहा। बड़ी मात्रा में विदेशी माल आने से चीन की सामंती अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से विघटित होने लगी। तब से चीन एक अर्द्ध-औपनिवेशिक और अर्द्ध-सामंती समाज में बदलता गया। चीनी राष्ट्रपति और विदेशी पूँजीपतियों के बीच का अंतर्विरोध धीरे-धीरे विकसित होकर प्रधान अंतर्विरोध बन गया। इसी समय से चीन के क्रांतिकारी आंदोलन का लक्ष्य भी दोहरा हो गया अर्थात घरेलू सामंती शासकों के विरूद्ध संघर्ष करने के साथ-साथ विदेशी पूँजीवादी आक्रमणकारियों का विरोध करना ।
अफीम युद्ध के बाद चीनी जनता विदेशी पूँजीपतियों और घरेलू सामंतवादी तत्वों के दोहरे उत्पीड़न का शिकार हो गई तथा उसके कष्ट बढ़ते गये। 1841 ई० से 1850 ई० के दौरान देश में 100 से अधिक किसान-विद्रोह हुए। 1851 ई० में अनेक छोटी-छोटी व्रिदोहरूपी धाराओं ने आपस में मिलकर एक प्रचंड प्रवाह अर्थात ताईपिंग विद्रोह का रूप ले लिया।
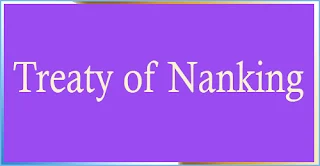 |
| Treaty of Nanking |
End of Articles.... Thanks...
Sunday, 9 October 2022
प्रथम अफीम युद्ध के कारणों एवं परिणामों
कारण - 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में चीन विश्व में एक अति धनाढ्य देश जाना जाता था। दुनिया से अलग-थलग वह एक सामंती समाजवाला देश था, जिसकी उत्पादन व्यवस्था में संयुक्त रूप से लघु-किसान कृषि और घरेलू दस्तकारी उद्योग की प्रधानता थी। काफी संख्या में किसान समुदाय के पुरूष खेतीबारी करते थे और स्त्रियाँ कताई बुनाई करती थीं। वे अपनी जरूरत का अनाज, कपड़ा और अन्य चीजें स्वयं ही पैदा कर लेते थे। प्रारंभ में चीन बड़े पैमाने पर सामान का निर्यात ही करता था और आयात छोटे पैमाने पर।
आर्थिक लाभ के लालच में यूरोप के कई देश चीन को ललचाई दृष्टि से देखते थे। 1840 ई० के आसपास ब्रिटेन संसार का सबसे विकसित पूँजीवादी देश था। भारत में अपना उपनिवेशवाद सुदृढ़ करने के फौरन बाद उसने चीन को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। ब्रिटेन में निर्मित सूती कपड़ा तथा ऊनी चीजें चीन के बाजार में आसानी से नहीं बिक पाती थीं। इसलिए ब्रिटिश पूँजीपतियों को चीन से चाय, रेशम और दूसरी उत्पादित वस्तुएँ खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में चाँदी अपने देश से यहाँ लानी पड़ती थी।
चाँदी के अभाव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीनी माल की कीमत चुकाने के लिए कोई अन्य उपाय सोचने लगी। उसने अफीम का व्यापार करने का फैसला किया। 1781 ई० में कंपनी ने पूरी तैयारी के साथ पहली बार भारतीय अफीम को बड़ी मात्रा में चीन भेजा। इससे पहले मादक द्रव्य के बारे में चीन के लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। इसके बाद यह व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। शीघ्र ही एक ऐसी हालत पैदा हो गई जिसमें चीन से निर्यात होनेवाली चाय, रेशम और अन्य चीजों का मूल्य चीन में आयात की जानेवाली अफीम का मूल्य चुकाने के लिए काफी नहीं रह गया तथा चाँदी देश के अंदर आने के बदले देश के बाहर जाने लगी।
1800 ई० ने चीन के सम्राट ने अफीम के शारीरिक और आर्थिक दुष्प्रभाव से अत्यंत चिंतित होकर चीन में इसपर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन, तबतक बहुत से लोगों को इसकी आदत लग चुकी थी। अफीम के व्यापार के मुनाफे से बहुत से व्यापारी और अफसर भ्रष्ट हो चुके थे। इसलिए तस्करी और घूसखोरी ने इस प्रतिबंध को लगभग निष्प्रभावी बना डाला।
अफीम का वार्षिक व्यापार, जो 1800 ई० में 2000 पेटियों के बराबर था, 1838 ई० में बढ़कर 40,000 पेटियों के बराबर हो गया। इस व्यापार में अमेरिकी जलयान काफी पहले ही शामिल हो चुके थे। वे भारतीय अफीम की कमी पूरी करने के लिए तुर्की की अफीम भी लाते थे। इस प्रकार, उन्होंने भी इस व्यापार में बेशुमार मुनाफा कमाया, जो बाद में अमेरिका के औद्योगिक विकास का आधार बना।
बेहद तेज गति से चीन की चाँदी बाहर जाने लगी। 1832-35 में दो करोड़ औंस चाँदी चीन से बाहर चली गई। परिणामस्वरूप, देश में उसका भाव बेहद चढ़ता गया। इसका बोझ किसानों पर पड़ा क्योंकि इससे अनाज के दाम गिरते गए। लेकिन, जमींदारों और कर वसूल करनेवालों ने पहले से अधिक अनाज वसूल करना शुरू कर दिया। इसलिए चाँदी के रूप में उनकी आमदनी पहले जैसी ही बनी रही। इस तरह चीन के सामंती समाज में तनाव पहले से ज्यादा बढ़ता गया। यह सामाजिक तनाव पहले हो इतना बढ़ चुका था कि अठारहवीं शताब्दी के मध्य में किसान विद्रोहों की एक नई लहर उठने लगी। 1810 ई० के बाद मंचू राजवंश के खिलाफ पहले से ज्यादा संख्या में और व्यापक पैमाने पर विद्रोह हुए। 1813 ई० में तो विद्रोहियों का एक दल पेकिंग में सम्राट के राजमहल में भी घुस गया।
अपने को बचाने के उद्देश्य से मंचू राजवंश के पेकिंग स्थित शासकों को मजबूर होकर कुछ कारगर कदम उठाने पड़े। अफीम के व्यापार की रोकथाम के लिए पहले से ज्यादा कड़े फरमान जारी करने के बाद, उन्होंने लिन चेश्वी को, जो अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध का पक्का समर्थक था, कैण्टन (क्वांगचो) का विशेष कमिश्नर नियुक्त कर दिया। लिन चेश्वी मार्च, 1839 में कैण्टन पहुँचा। जनता के समर्थन में उसने नगर के उस भाग की नाकेबंदी कर दी जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकी व्यापारियों को अपने व्यापारिक संस्थान कायम करने की अनुमति थी। उसने वहाँ के तमाम अफीम व्यापारियों को आदेश दिया कि वे अफीम का अपना सारा स्टॉक एक निश्चित अवधि के अंदर उसके हवाले कर दें। इस आदेश के बाद चीन स्थित ब्रिटिश व्यापार अधीक्षक चार्ल्स इलियट को 20,000 पेटियों से ज्यादा अफीम, जिसका वजन 11 लाख 50 हजार किलोग्राम था, चीनी अधिकारियों के हवाले करना पड़ा। इनमें लगभग 1,500 पेटियाँ अमेरिकी व्यापारियों की थीं। 3 जून, 1839 को लिन चेश्वी ने एक अन्य आदेश जारी किया कि जब्त की हुई तमाम अफीम हूमन कं समुद्रतट पर खुलेआम जला दी जाए। इस तरह तमाम अफीम जला देने के बाद लिन चेश्वी ने चीन और ब्रिटेन के बीच का सामान्य व्यापार पुनः शुरू करने का आदेश दिया। इसके साथ यह प्रतिबंध भी लगा दिया कि आगे से ब्रिटिश व्यापारियों को किसी भी हालत में थोड़ी-सी भी अफीम चीन में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिणामस्वरूप, पहला अफीम युद्ध छिड़ गया।
परिणाम - ब्रिटेन चीन में अपना अवैध अफीम-व्यापार जारी रखने पर तुला हुआ था, इसलिए 1840 ई० में उसने चीन के विरूद्ध पहला अफीम युद्ध छेड़ दिया। चीनी जनता हमलावरों के विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने के लिए उठ खड़ी हुई। किंतु, भ्रष्ट छिंग सरकार ने विदेशी दुश्मन के सामने घुटने टेक देना ही बेहतर समझा। उसे डर था कि यदि अँगरेजों के विरूद्ध लड़ाई जारी रही तो देश की जनता उसमें भाग लेकर पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और तब स्वयं छिंग सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।
युद्ध के परिणामस्वरूप चीन पर प्रथम बार अपमानजनक 'असमान संधियाँ' थोप दी गई। इन संधियों ने चीन को राष्ट्रीय विनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया। छिंग शासकों ने 1843 ई० में ब्रिटेन के साथ नानकिंग की साँध पर हस्ताक्षार कर दिए। 1843 ई० की संधि के अनुसार- (a) लिन चेश्वी द्वारा जब्त की गई और जलाई गई अफीम की क्षतिपूर्ति करनी होगी। यह इस विषैले पदार्थ के सभी भावी व्यापारियों के लिए सुरक्षा का आश्वासन था।
(b) हांगकांग ब्रिटेन को दे देना होगा। बाद में चलकर हांगकांग का प्रयोग ब्रिटेन ने चीन में अपनी सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक के अड़े के रूप में किया।
(c) पाँच मुख्य बंदरगाहों को ब्रिटिश व्यापार एवं ब्रिटिश बस्तियों के लिए खोलना होगा। इससे शीघ्र ही ब्रिटेन के प्रभुत्ववाले प्रादेशिक क्षेत्र कायम हो गए। ये प्रादेशिक क्षेत्र चीन के बंदरगाहों की तथाकथित विदेशी बस्तियों के प्रारंभिक रूप थे।
(d) ब्रिटिश नागरिकों पर चीनी कानून लागू नहीं होंगे। इससे अन्य देशों को भी चीन की प्रादेशिक भूमि पर विदेशी कानून लागू करने की अनुमति मिल गई।
(e) चीन को ब्रिटेन का कृपापात्र बनकर रहना होगा। इसकी माँग अन्य शक्तियों द्वारा भी की गई और इस प्रकार सभी विदेशियों को वे 'विशेषाधिकार' प्राप्त हो गए जिन्हें ब्रिटिश आक्रमणकारियों ने चीन से ऐंठ लिया था।
(f) चीन विदेशी माल पर 5 प्रतिशत से ज्यादा आयात कर न लगाने का वचन देगा। यह चीन के घरेलू उद्योग के विकास के लिए घातक साबित हुआ।
चीन को निर्बल देख अन्य विदेशी शक्तियों के दूत भी अपने नौपोतों पर सवार होकर ऐसी ही सौंधयाँ थोपने आ पहुँचे। पहला दूत संयुक्त राज्य अमेरिका से आया जिसका नाम था कालेव कुशिंग। उसने कमजोर पैकिंग दरबार को लापरवाह ढंग से सूचित किया कि यदि उसने समझौता वार्ता से इनकार किया तो इसे 'राष्ट्रीय अपमान और युद्ध का न्यायोचित कारण' समझा जाएगा। 1844 ई० में चीनी सरकार की वांगश्या संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी दूत कुशिंग ने बाध्य कर दिया। इस संधि के अनुसार चीन के सामंती शासकों ने जितना विशेषाधि कार ब्रिटेन को दिया था उससे अधिक विशेषाधिकार अमेरिका को प्राप्त हुआ। कुशिंग की यह संधि व्यवहार में तस्करों के लिए वरदान सिद्ध हुई।
अमेरिका के साथ हुई सौंध को देख ब्रिटेन ने चीन से और कुछ प्राप्त करना चाहा। 1847 ई० में उसने चीन पर दबाव डाला कि ब्रिटेन द्वारा शासित भारत और पश्चिमी तिब्बत के बीच की सीमा को औपचारिक रूप से निर्धारित कर दिया जाए, ताकि अपने इच्छानुसार वह जो सीमा रेखा चाहे चीन पर थोप सके। तिब्बत में घुसपैठ करने और उसे चीन से अलग करने का हर विदेशी प्रयास समूचे चीन पर साम्राज्यवादियों के आक्रमण की प्रक्रिया और विभाजन के प्रयास का ही एक अभिन्न अंग था।
अफीम युद्ध के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ईसाई मिशनरियों ने चीन की स्थिति और चीनी भाषा की जानकारी का फायदा उठाकर चीन को अपमानित करने का प्रयास किया; जबकि चीन में वे केवल ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे।
डॉ० गुत्जलाफ नामक एक पादरी ने ब्रिटिश अफीम कंपनी को बिचौलिए के रूप में काम किया था तथा पुरस्कार के रूप में अपनी धार्मिक पत्रिका के लिए अनुदान प्राप्त किया था। वह बाद में चलकर ब्रिटिश फौज का दुभाषिया और गुप्तचर संगठनकर्ता बन गया। ब्रिटेन के लिए गुप्तचरी करने के लिए उसने चीनी जासूस भर्ती किए थे। ब्रिटिश सेना ने जब तिंगहाउ नगर आदि पर अधिकार कर लिया तब निंगपो नामक बंदरगाह का प्रशासक गुत्जलाफ को बनाया गया। बाद में वह हांगकांग की ब्रिटिश सरकार में 'चीनी मामलों का सचिव' बन गया।
अमेरिका के साथ हुई वांगश्या संधि के दौरान भी अमेरिको ईसाई मिशनरी विलियम्स, ब्रिजमैन और पार्कर ने ही अमेरिकी दूत कुशिंग को सलाह दी थी कि वह एक ऐसा रूख अपनाए जिससे चीन 'झुक जाए या टूट जाए।
युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने सभी को यह आश्वासन दिया कि यह लड़ाई अफीम के लिए नहीं बल्कि चीन को यह सिखाने के लिए की जा रही थी कि वह प्रगति और स्वतंत्र व्यापार का विरोध न करे। 1850 ई० में भारत की ब्रिटिश सरकार को अफीम के व्यापार से होनेवाला मुनाफा उसके कुल राजस्व के 20 प्रतिशत तक पहुँच गया, जबकि चीन इस व्यापार के कारण शक्तिहीन एवं निर्धन बनता गया।
चीन में अफीम का 'कानूनी' आयात 1917 ई० तक जारी रहा। चीन की भूमि पर विदेशियों को प्राप्त प्रशासनिक रियायतों को और अधिक विस्तार व आक्रमण करने के लिए स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया। देश का घरेलू बाजार विदेशी माल से पाट दिया गया। चीन एक अर्द्ध औपनिवेशिक एवं अर्द्ध-सामंती देश बन गया।
विदेशी हमलावरों को हजनि को बहुत बड़ी रकम भुगतान करने के लिए देश की जनता से छिंग सरकार ने हर तरह से धन ऐंठना शुरू किया। जनता कराह उठी और चीन के इतिहास में सबसे बड़े क्रांतिकारी किसान आंदोलन की तस्वीर बनी।
 |
| First Opium War |
Tuesday, 20 September 2022
मेइजी संविधान के प्रमुख प्रावधान
मेइजी संविधान सन् 1888 ई० तक बनकर तैयार हो चुका था और अगले वर्ष सन् 1889 ई० में इसे लागू कर दिया गया। नये विधान में जापानी जनता की सम्राट के प्रति अन्य भक्ति की भावना का आदर करते हुए सम्राट को शासन का अधिपति व मुखिया बनाया गया, उसकी स्थिति पवित्र व अनुल्लंघनीय' रखी गई। विविध उच्चाधिकारियों की नियुक्ति, उनका वेतन निर्धारण तथा उनकी पदच्युति का अधिकार सम्रट को था। युद्ध व शांति की घोषणा सम्राट हो कर सकता था। विशेष परिस्थितियों में सम्राट अध्यादेश जारी कर सकता था। कोई भी विष "येक तब तक प्रभावकारी नहीं हो सकता था जब तक सम्राट अपने हस्ताक्षरों द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान न कर दें। सम्राट अपने इन अधिकारों का प्रयोग दो वैधानिक परामर्शदात्री समितियों (मंत्रिपरिषद् तथा प्रिवी कौंसिल जिनका गठन विधान के पूर्व हो चुका था) के माध्यम से करते थे। मंत्रि-परिषद् और प्रिवी कौंसिल के सदस्यों को सम्राट मनोनीत करता था और वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। पार्लियामेंट के प्रति उन्हें उत्तरदायी नहीं बनाया गया था, सम्राट के विश्वास प्राप्त रहने तक ही ये लोग अपने पदों पर रह सकते थे।
इस नये विधान की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके द्वारा जापान में पार्लियामेंट की स्थापना की गई। जापानी डायट के दो सदन थे उच्च सदन (लार्ड सभा) तथा निम्न सदन (लोक सभा)- उच्च सदन में राजघराने के व्यक्ति, प्रिंस, माक्विंस, काउन्ट, वाइकाउन्ट तथा बैरन वर्ग के प्रतिनिधि कुलीन, सम्राट द्वारा मनोनीत सदस्य एवं सबसे अधिक राजकीय कर देने वाले लोग होते थे। निम्न सदन में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते थे, परन्तु सन् 1889 ई० में मताधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया था। मताधिकार के लिए सम्पत्ति की शर्त रखी गई थी। किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, जापान में मताधिकार भी विस्तृत होता गया। पार्लियामेंट के अधि वेशन को वर्ष में कम से कम एक बार बुलाना आवश्यक था। नये करों को लगाने तथा नये बजट के लिए पार्लियामेंट की स्वीकृति आवश्यक थी। सम्राट् को यह अधिकार था कि वह पार्लियामेंट में स्वीकृत किसी भी कानून के विरूद्ध अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सके। पार्लियामेंट के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते थे और उनके विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते थे किन्तु मंत्रियों को बर्खास्त करने का अधिकार केवल सम्राट् को था । पार्लियामेंट के सदस्यों को भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता थी।
नये शासन विधान में नागरिकों के अधिकारों का विशद् रूप से प्रतिपादन किया गया था। कानून की दृष्टि से जापानी एक समान थे। राजकीय पद, नौकरी, भाषण, लेखन सभाएँ करने, संगठन बनाने, अपने विचारों को प्रकट करने तथा अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की सबको स्वतंत्रता दी गई थी। राजकर्मचारियों को स्वेच्छापूर्वक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार न था। अभियुक्तों पर न्यायालय में मुकदमा चलाने तथा न्यायालय से दण्ड पा जाने के बाद जेल में रखा जा सकता था अन्यथा नहीं। अधिकारों को कानून द्वारा सीमित भी किया जा सकता था।
इटों को संविधान निर्माण करते समय यह चिन्ता थी कि जापान के नेताओं के हाथों में शक्ति केन्द्रीभूत रहे। इसके लिए वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के एक संगठन का विधान में बाद में आयोजन किया गया। सामन्ती युग की याद दिलाने वाले जनेरो में वे शक्तिशाली नेता थे जिन्होंने संक्रमण काल - में राष्ट्र का नेतृत्व किया था। यह संगठन मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति तथा युद्ध और शांति सरीखे बड़े-बड़े प्रश्नों पर सम्राट को सलाह देता था।
इस नये विधान का वित्त सम्बन्धी छठा अध्याय सबसे अधिक रूचिकर एवं उत्तरदायी शासन की जड़ों पर सबसे अधिक प्रहार करने वाला था । यद्यपि बजट या वार्षिक आय-व्यय के प्रभावकारी होने के लिए निम्न सदन की सहमति आवश्यक थी किन्तु इस सदन को वास्तविक वित्तीय अधिकार या नियंत्रण बिल्कुल नहीं दिया गया था। सदन के इस अधिकार का अपहरण यही सावधानी से किया गया था। देश की कर प्रणाली विधान लागू होने के पूर्व ही बन चुकी थी, इसलिए में यह व्यवस्था की गई कि चालू करों में संशोधन करने या नये करों के लगाने के लिए पार्लियामेंट को स्वीकृति आवश्यक होगी। प्रशासकीय शुल्कों, मुआवजों तथा क्षतिपूर्तियों के रूप में कुछ ऐसी राजतंत्र आय की व्यवस्था की गई, जो पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी गई। व्यय के सम्बन्ध में कहा गया कि 'विधान द्वारा प्रदत्त सम्राट् के अधिकारों पर आधारित व्ययों (जैसे कि वेतन) या कानूनों को लागू करने के परिणामस्वरूप होने वाले खर्च या शासन के वैध उत्तरदायित्वों पर होने वाले व्ययों को पार्लियामेंट प्रशासन की सहमति के बिना न तो कम कर सकती है और न ही अस्वीकार। आकस्मिक व्ययों के लिए सुरक्षित निधि की व्यवस्था तथा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशासन पार्लियामेंट से धन की माँग कर सकता था। यह भी व्यवस्था की गई थी कि यदि पार्लियामेंट नये बजट को स्वीकार करने से मना कर दे, तो पिछले बजट के अनुसार वित्तीय व्यवस्था की जा सकेगी। इस प्रकार पार्लियामेंट का एकमात्र वित्तीय अधिकार यह रह गया था कि वह खर्च का बढ़ना रोक सकती थी।
सन् 1889 ई० के शासन-विधान द्वारा जापान राजनीतिक तथा शासन की दृष्टि से पाश्चात्य देशों के निकट पहुँच गया था। यद्यपि फ्रांस, अमेरिका तथा ब्रिटेन लोकतंत्रवाद की दृष्टि से जापान से काफी आगे थे किन्तु जर्मनी, आस्ट्रिया तथा स्पेन सरीखे कुछ ऐसे भी राष्ट्र थे जो जापान से अधिक उन्नत नहीं थे। रूस, टर्की आदि की सरकारें जापान की अपेक्षाकृत निश्चित रूप से अधिक निरंकुश व स्वेच्छाचारी थी। यूरोप के राष्ट्रों को सामन्त पद्धति एवं एकतंत्र शासन का अन्त कर लोकतंत्र तक पहुँचने में सदियों लगी थी, पर जापान ने चौथाई शताब्दी से कम में ही सामन्त पद्धति तथा निरंकुश शासन का अन्त कर एक ऐसे संविधान की रचना की जो 19वीं शती की प्रवृत्तियों के अनुकूल था। वैधानिक आन्दोलन के इस वर्णन से स्पष्ट है कि जापान में प्रजातंत्र का जन्म ‘अनायास विस्फोट या क्रांति से नहीं वरन् विकास की प्रक्रिया द्वारा हुआ है।
यद्यपि संविधान की घोषणा सन् 1889 ई० में हुई किन्तु विधान पूर्ण रूप से सन् 1890 ई० में लागू हुआ जबकि पहली डायट का संगठन और अधिवेशन आरम्भ हुआ। चुनावों के होते ही भविष्य के मतभेदों की रूपरेखा स्पष्ट हो गई। निम्न सदन में राजनीतिक दलों का तथा मंत्रि-परिषद् पर कुल के नेताओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। डायट के पास इतने अधिकार तो थे ही कि वह किसी भी कार्य में बाधा डाल सके किन्तु नियंत्रण के अधिकार उसके पास न थे। शासन ने इन दो अंगों डायट व मंत्रि-परिषद् के बीच मतभेदों को दूर करने की व्यवस्था संविधान में न थी। सम्राट् के पास अपील और उसके निर्णयात्मक घोषणा द्वारा ही इस संघर्ष का निराकरण हो सकता था। मंत्रि-परिषद् में मनोनीत कुल नेताओं के सम्मुख शासन चलाने के लिए एक ही रास्ता था कि या तो वे डायट पर नियंत्रण करें या डायट द्वारा उपस्थित गतिरोध की चिन्ता न करते हुए शासन चलाते रहें। समस्या का असली समाधान था मंत्रि-परिषद् का डायट के प्रति उत्तरदायी होना, किन्तु इस समस्या पर किसी ने विचार नहीं किया था। अधिकारी तंत्र- जेनरो तथा मंत्रि-परिषद् ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रतिनिधि सभा को बार-बार भंग कराकर नए चुनाव कराये ताकि उनके समर्थक प्रतिनिधि सभा (निम्न सदन) में बहुसंख्या में आ सके। नये संविधान के लागू होने के चार वर्षों बाद तक मंत्रिपरिषद को विरोधी प्रतिनिधि सभा का सामना करना पड़ा। तीन बार मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन हुआ। कई बार डायट भी भंग की गई।
 |
| Major Provisions of the Meiji Constitution |
End of Articles..... Thanks....
Thursday, 4 August 2022
वियतनाम युद्ध की विवेचना
पृष्ठ भूमि - द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया सम्मिलित रूप से फ्रांस का हिंदचीन नामक उपनिवेश था। द्वितीय विश्वयुद्ध में हिंदचीन के अनेक भागों पर जापान का अधिकार हो गया। इसके पूर्व से ही हिंदचीन में फ्रांस से मुक्त होने के लिए आंदोलन चल रहा था।
जापान का विरोध - हो-ची-मिन्ह वियतनाम के सबसे लोकप्रिय नेता थे। उन्हीं के नेतृत्व में वियतनामी जनता ने जापानी कब्जे का विरोध किया और वियतमिन्ह नाम से एक जनसेना का संगठन किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने तक वियतनाम के बड़े हिस्से पर वियतमिन्ह का नियंत्रण हो चुका था। अगस्त, 1945 में राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के नेतृत्व में स्वतंत्र वियतनाम गणतंत्र की घोषणा हुई।
फ्रांस के साथ युद्ध - अक्टूबर, 1945 में वियतनाम पर पुनः अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी सेना वहाँ आ गई। 1946 ई० में फ्रांसीसी सेना तथा वियतनाम की वियतमिन्ह सेना में युद्ध छिड़ गया। फ्रांस ने बाओ-दाई के नेतृत्व में वहाँ एक कठपुतली सरकार भी बैठा दी। फ्रांस और वियतनाम का युद्ध लगभग आठ वर्षों तक चला। 1954 ई० में वियतनाम की सेना वियतमिन्ह नै दिएन बिएन-फू के किले के पास फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। दिएनबिएन-फू में फ्रांसीसियों की पराजय की चर्चा काफी दिनों तक होती रही क्योंकि बिना आधुनिक शस्त्रों के एक जनसेना वियतमिन्ह ने फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध में हरा दिया था।
जेनेवा का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और वियतनाम का विभाजन - 1954 ई० में जेनेवा में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इसके निर्णय के अनुसार वियतनाम को दो भागों में बाँट दिया गया-उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। साथ ही, दो वर्षों के भीतर वियतनाम के एकीकरण के लिए चुनाव करने का भी निश्चय किया गया। लाओस और कम्बोडिया को भी स्वतंत्र कर दिया गया।
अमेरिका के साथ युद्ध - वियतनाम के विभाजन के बाद वहाँ स्वतंत्र आंदोलन का एक नया दौर शुरू हुआ। विभाजन संबंधी समझौते के अनुसार उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बनी और दक्षिणी वियतनाम में न्यो-पिन्ह-वियम ने शासन संभाला। पर, अमेरिका के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम में बनी सरकार ने जेनेवा सम्मेलन के चुनाव कराने और वियतनाम के एकीकरण के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। फलत:, 1960 ई० में दक्षिणी वियतनाम की सरकार के विरूद्ध जन आंदोलन आरंभ हो गया। वहाँ की जनता ने 'कांग' नामक एक संगठन बनाया और सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद वियतनाम सरकार ने वियतनाम में बड़े पैमाने पर सैनिक हस्तक्षेप किया। दक्षिणी वियतनाम के आंदोलन को दबाने के लिए अमेरिका ने आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से लैश लाखों सैनिकों को वहाँ भेज दिया। दक्षिणी वियतनाम की जनता ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में छापामार युद्ध आरंभ कर दिया। दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम का भी समर्थन प्राप्त था। अतः अमेरिकी सेना ने उत्तरी वियतनाम में भी युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में अमेरिकी सेनाओं को भारी बम वर्षा के कारण वियतनाम की बड़ी क्षति हुई। अमेरिकी सेनाओं ने कीटाणु युद्ध के अस्त्रों का भी उपयोग किया।
वियतनाम द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति - इस युद्ध के प्रश्न पर अमेरिका दुनिया के लगभग सभी देशों से पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया। कई देशों ने अमेरिका की कार्रवाई की तीव्र निंदा की स्वयं अमेरिका में भी इस युद्ध का विरोध हुआ। 1975 ई० के आरंभ में युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर आया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की सेनाएँ पूरे देश पर छा गई। उन्होंने दक्षिणी वियतनाम सरकार की समर्थित सेनाओं का सफाया कर दिया। इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 54 हजार सैनिक मारे गए। इसके बाद अमेरिकी सेना वियतनाम से हटने लगी और 30 अप्रैल, 1975 तक सारी अमेरिकी सेना हट गई। इसके बाद दक्षिणी वियतनाम की राजधानी सैगोन को मुक्त करा लिया गया।
वियतनाम का एकीकरण - 1976 ई० में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम औपचारिक रूप से मिलकर एक हो गए। सैगोन शहर का नाम महान वियतनामी नेता हो-ची-मिन्ह की स्मृति में हो-ची-मिन्ह नगर रखा गया।
वियतनाम के एकीकरण तथा स्वतंत्रता प्राप्ति का महत्व - उत्तरी और दखिणी वियतनाम के एकीकरण तथा उनका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। एक छोटे से देश ने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति की सेना का डटकर मुकाबला करने और उसे पराजित करने के बाद पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त की थी तथा अपना एकीकरण किया था। अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले देशों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।
अमेरिका के हस्तक्षेप के समाप्त होने पर वियतनाम को एक और युद्ध करना पड़ा। फ्रांस तथा अमेरिका के विरूद्ध स्वाधीनता के लिए वियतनाम और कंबोडिया तथा लाओस की जनता ने मिलकर युद्ध किया था। अमेरिका की सेना के कटने के बाद वियतनाम और कंबोडिया स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए।
कंबोडिया में पोलपोट के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। इस सरकार ने कंबोडिया की जनता पर अत्याचार करना शुरू किया और नरसंहार की नीति अपनाने लगी। ऐसा अनुमान है। कि लगभग तीस लोगों को मार दिया गया। 1979 ई० में वियतनाम की सरकार कंबोडिया की जनता की मदद के लिए आगे आई। उसकी सहायता से पोलपोट की सरकार को हटा दिया गया। पर, पोलपोट की सेना ने थाइलैंड से मिली सीमा के दूसरी ओर से युद्ध करना जारी रखा। हाल में वियतनाम की सेना कंबोडिया से हट गई है और वहाँ शांति की स्थापना हेतु बातचीत जारी है। पोलपोट की सरकार को चीन का समर्थन प्राप्त था। 1979 ई० में चीन ने वियतनाम पर भी आक्रमण किया था, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली।
 |
| Vietnam War Review |
End of Articles.... Thanks....