Sunday, 28 December 2025
Friday, 17 November 2023
कंकाल तंत्र
मानव शरीर में हड्डियों की व्यवस्था को कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाता है।
Bones (हड्डी)
1. हड्डियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है,
2. हड्डियों के रोग का अध्ययन करना ऑर्थोलोजी कहलाता है।
3. हड्डी एक प्रकार की ऊतक (Tissue) है जो कई कोशिकाओं से मिल कर बनी होती है
4. हड्डी मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक होती है।
5. नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है।
6. वयस्कों में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है।
7. हड्डियों का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा Ossein प्रोटीन से मिलकर बना होता है।
8. हमारी हड्डी में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है
- ओस्टेओसीटे (Osteocyte) कोशिका जो हमारी हड्डी बनाती है।
- ओस्टेओक्लास्ट (Osteoclast) कोशिका जो हमारी हड्डी की मरम्मत करती है
- हड्डी रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है।
- वसा हमारी हड्डी के वसीय ऊतक (Adipose Tissue) में संगृहीत हो सकती है।
- खनिजों का संग्रहण
- अंगो को सुरक्षा प्रदान करना
- हड्डी हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती है।
- अक्षीय कंकाल तंत्र (Arial Skeletal System)
- कुल हड्डियां - 80
- उपांगीय कंकाल तंत्र (Appendicular Skeletal System)
- कुल हड्डियां - 126
- खोपड़ी की हड्डी - 29
- कपाल (Cranium) की हड्डी - 8
- चेहरे की हड्डी - 14
- कान की हड्डी 6
- गले की हड्डी - 1
- पसलियां + 1 हड्डी
- पसली (Ribs) = 12 जोड़ी (24+1= 25) हड्डी
- 1 से 7 कशेरुकी (Cervical Curve/Spine) = 7
- 8 से 19 कशेरुकी (Thorasic Spine) वक्षीय = 12
- 20-24 कशेरुकी (lumbar) = 5
- 25 वीं कशेरुकी (Sacrum) = 1
- 26 वीं कशेरुक पूंछ = 1
- Sphenoid Bone तितली का आकर, यह बाकी की 7 हड्डियों को स्पर्श करती है, Key Stone of Cranium (प्रधान हड्डी)
- Ethmoid bone plate के आकार की हड्डी होती है
- Frontal bone - 1
- Temporal bone - 2
- Parietal Bone - 2
- Ocipital Bone - 1
- Ethmoid Bone - 1
- Sphenoid Bone - 1
- नाम - हायोड (hyoid)
- आकार - U
- जीभ को पकड़कर रखने वाली हड्डी
- कुल पसलियां = 12 जोड़ी + 1 छाती की हड्डी (Sterrrium)
- 1 से 7 जोड़ी - सत्य पसली (True Ribs)
- 8-9-10 वी जोड़ी false ribs
- 11 - 12 वीं - Floating Ribs (घुमावदार पसली)
- Frontal Attachment of ribs (आगे से जुडी हुई) Sternum
- Dorsal attachment of ribs (पीछे से जुडी हुई)-- (Back Bone)
- रीढ़ की हड्डी
- चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी Maxilla (ऊपरी जबड़े की हड्डी)
- Nasal Bone (नाक की हड्डी) = 2
- Lacrimal Bone (आंख में स्थित) = 2
- Palatine Bone (Buccal cavity)= 2
- Zygomatic Bone (गाल की हड्डी) = 2
- Vomer Bone (नाक के बीच की हड्डी) = 1
- Maxilla Bone (ऊपरी जबड़ा) - 2
- Mandible Bone (निचला जबड़ा) - 1
- Inferior nasal concha bone = 2
- Melius
- Incus
- Stapes - मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है।
Friday, 12 May 2023
| राशि | मात्रक(S.I) | प्रतीक |
| लम्बाई | मीटर | m |
| द्रव्यमान | किलोग्राम | kg |
| समय | सेकेंड | s |
| कार्य तथा ऊर्जा | जूल | J |
| विधुत धारा | एम्पियर | A |
| ऊष्मागतिक ताप | केल्विन | K |
| ज्योति तीव्रता | कैण्डेला | cd |
| कोण | रेडियन | rad |
| ठोस कोण | स्टेरेडियन | sr |
| बल | न्यूटन | N |
| क्षेत्रफल | वर्गमीटर | m2 |
| आयतन | घनमीटर | m3 |
| चाल | मीटर प्रति सेकेण्ड | ms-1 |
| कोणीय वेग | रेडियन प्रति सेकेण्ड | rad s-1 |
| आवृत्ति | हर्ट्ज | Hz |
| जड़त्व आघूर्ण | किलोग्राम वर्गमीटर | kgm2 |
| संवेग | किलोग्राम मीटर प्रति सेकेण्ड | kg ms-1 |
| आवेग | न्यूटन - सेकण्ड | Ns |
| कोणीय संवेग | किलोग्राम वर्गमीटर प्रति सेकेण्ड | kgm2s-1 |
| दाब | पास्कल | Pa |
| शक्ति | वाट | W |
| पृष्ठ तनाव | न्यूटन प्रति मीटर | Nm-1 |
| श्यानता | न्यूटन सेकेण्ड प्रति वर्ग मीटर | Nsm-2 |
| ऊष्मा चालकता | वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेण्टीग्रेड | Wm-1 oC-1 |
| विशिष्ट ऊष्मा | जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन | J kg-1K-1 |
| विधुत आवेश | कूलॉम | C |
| विभवान्तर | वोल्ट | V |
| विधुत प्रतिरोध | ओम | Ω |
| विधुत धारिता | फैराड | F |
| प्रेरक | हेनरी | H |
| चुम्बकीय-फ्लक्स | बेवर | Wb |
| ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन | lm |
| प्रदीप्ति घनत्व | लक्स | lx |
| तरंगदैर्ध्य | ऐंग्स्ट्रम | Å |
 |
| Various Units of Measurement and Weight |
Saturday, 15 April 2023
जिस प्रकार शरीर की संरचना हाथ पाँव, नाक, कान, आँख एवं मुँह आदि कई अंगों अथवा इकाइयों से मिलकन बनी होती है। ठीक इसी प्रकार से समाज की संरचना भी होती है। प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये इकाइयों परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित होती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों अथवा इकाइयों से मिलकर होता है। इन इकाइयों में परस्पर स्थायी एवं व्यवस्थित सम्बन्ध पाये जाते हैं। ये अंग अथवा इकाइयाँ स्थिर रहती हैं। संरचना का सम्बन्ध बाहर की आकृति व स्वरूप से होता है। उसका संबंध आन्तरिक रचना से नहीं होता है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। समाज की संरचना भी शरीर की तरह ही कई इकाइयों, जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानों, मूल्यों एवं पदों आदि से बनी होती है।
सामाजिक संरचना का अर्थ व परिभाषायें विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो सामाजिक संरचना की परिभाषायें दी हैं, उनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं-
1. मैकाइवर एवं पेज के अनुसार “समूहो के विभिन्न प्रकारों से मिलकर सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण होता है।"
2. मजूमदार एवं मदान के अनुसार "पुनरावृत्तीय सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है।"
3. टाल कॉट पारसन्स के अनुसार "सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेन्सियों और सामाजिक प्रतिमानों तथ साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किये गये पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं।'
4. कार्ल मानहीम के अनुसार "सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिसमें अवलोकन और चिन्तन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है।'
5. जिन्स वर्ग के अनुसार "सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात् समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इन सबके संकुल जिससे कि समाज का निर्माण होता है, से संबंधित हैं। "
6. एच. एम. जोनसन के अनुसार "किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों के अपेक्षाकृत स्थायी अन्तर्सम्बन्धों से निर्मित होती है, स्वयं 'अंग' शब्द से ही कुछ स्थायित्व के अंग का ज्ञापन होता है। सामाजिक प्रणाली क्योंकि लोगों के अन्तर्सम्बन्धित कृत्यों से निर्मित होती हैं, इसकी संरचना भी इन कृत्यों में पायी जाने वाली नियमितता या पुनरावृत्ति के अंशों में ढूँढी जानी चाहिए।"
7. ब्राउन के अनुसार "सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही है, और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है।"
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों एवं सामाजिक सम्बन्धों से निर्मित एक प्रतिमार्वनत एवं क्रमबद्ध ढाँचा है। इस प्रकार सामाजिक संरचना अपेक्षतया एक स्थिर अवधारणा है। जिसमें परिवर्तन अपवादस्वरूप ही देखने को मिलते हैं।
सामाजिक संरचना की विशेषताएँ (Characteristics of Social Structure)
सामाजिक संरचना की अवधारणा को इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है-
1. सामाजिक संरचना एक क्रमबद्धता है : इसका तात्पर्य यह है कि जिन इकाइयों 8 के द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, वे एक क्रमबद्धता में व्यवस्थित होती है। यही क्रमबद्धता सामाजिक संरचना के एक विशेष प्रतिमान को स्पष्ट करती है।
2. सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी होती है : इसे स्पष्ट करते हुए जॉन्सन ने लिखा है कि सामाजिक संरचना का निर्माण जिन समूहों तथा संघों से होता है, उनकी प्रकृति कहीं अधिक स्थायी होती है। उदाहरण के लिए, परिवार में यदि कर्ता या किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाय तो भी संयुक्त परिवार की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता।
3. सामाजिक संरचना की अनेक उप-संरचनाएँ होती हैं: सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों की संरचना को उनकी उप-संरचना कहा जाता है। उदाहरण के लिए, राज्य, सरकार, राजनीतिक दल तथा दबाव समूह एक राजनीतिक संरचना की उप-संरचनाएँ हैं। इसी तरह पंचायत, युवागृह तथा नातेदारी व्यवस्था, जनजातीय सामाजिक संरचना की उप-संरचनाएँ हैं। सांस्कृतिक संरचना का निर्माण करने में बहुत-सी परम्पराओं, प्रथाओं तथा मूल्यों का समावेश होता है तथा इन सभी की अपनी उप-संरचनाएँ होती हैं। यह सभी उप-संरचनाएँ मिलकर एक विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण करती है।
4. सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग परस्पर संबंधित होते हैं: यदि उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर देखा जाये तो स्पष्ट होता है कि नातेदारी की संरचना शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक और मनोरंजनात्मक उप-संरचनाओं से संबंधित होती है। इसी तरह व्यक्ति के समाजीकरण में परिवार, विद्यालय, धर्म, सरकार, राजनीतिक दलों तथा आर्थिक उप-संरचनाओं का समान योगदान होता है। इस प्रकार सभी उप-संरचनाएँ एक-दूसरे से संबंधित रहकर किसी सामाजिक संरचना को उपयोगी और प्रभावशाली बनाती हैं।
5. सामाजिक संरचना में मूल्यों का समावेश होता है : इसका तात्पर्य यह है कि व्यवहार और सम्मान के अनेक तरीके, जनरीतियाँ, प्रथाएँ, परम्पराएँ तथा प्रतीक इसका निर्धारण करते हैं कि किसी सामाजिक संरचना की प्रकृति किस प्रकार की होगी। विभिन्न समाजों के सामाजिक मूल्य एक-दूसरे से भिन्न होने के कारण ही उनकी सामाजिक संरचना में एक स्पष्ट अन्तर दिखायी देता है।
6. सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के निर्धारित प्रकार्य होते हैं: इन प्रकार्यों का निर्धारण सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक प्रतिमानों के द्वारा होता है। इन मूल्यों और प्रतिमानों में साधारणतया कोई परिवर्तन न होने के कारण भी सामाजिक संरचना की प्रकृति तुलनात्मक रूप से स्थायी हो जाती है।
7. सामाजिक संरचना अमूर्त होती है : पारसन्स ने लिखा है कि सामाजिक संरचना कोई वस्तु अथवा व्यक्तियों का संगठन नहीं है, बल्कि यह केवल अनेक इकाइयों की कार्यविधियों और उनके पारस्परिक संबंधों का एक प्रतिमान है। मैकाइवर का कथन है कि जिस प्रकार हम समाज को देख नहीं सकते, उसी तरह सामाजिक संरचना भी एक अमूर्त अवधारणा है। यह सत्य है कि परिवार, गाँव, जाति, वर्ग, राज्य तथा विभिन्न समितियाँ और संस्थाएँ सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयाँ हैं किन्तु सामाजिक संरचना का तात्पर्य इन इकाइयों के बाहरी रूप से न होकर उस क्रमबद्धता से है जो समाज के एक विशेष प्रतिमान को स्पष्ट करती है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना की प्रकृति अमूर्त होती है।
8. सामाजिक संरचना का तात्पर्य सदैव संगठन से नहीं होता : यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सामाजिक व्यवस्था संगठन का बोध कराती है परन्तु सामाजिक संरचना में कुछ व्यक्ति अथवा इकाइयाँ भी हो सकती हैं जिनके व्यवहार सामाजिक नियमों के प्रतिकूल हो। इसे मर्टन ने सामाजिक नियमहीनता' कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना का संबंध केवल सामाजिक संगठन की दशा से ही नहीं होता, बल्कि इसमें उन सभी दशाओं का समावेश होता है जो संगठन और विघटन के तत्वों का बोध कराती हैं।
9. सामाजिक संरचना स्थानीय आवश्यकताओं से प्रभावित होती है : वास्तव में, एक विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण उसकी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक आवश्यकताओं के आधार पर होता है। जब कभी इन दशाओं अथवा आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है, तब सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली उप-संरचनाओं में भी कुछ परिवर्तन होने लगता है, यद्यपि सम्पूर्ण संरचना में जल्दी ही कोई परिवर्तन नहीं होता।
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना का एक वाह्य रूप है जिसके निर्माण में बहुत-से समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक मूल्यों का योगदान होता है। इन सभी इकाइयों की प्रकृति का निर्धारण एक विशेष संस्कृति पर आधारित होने के कारण ही सामाजिक संरचना को अक्सर सांस्कृतिक संरचना भी कह दिया जाता है।
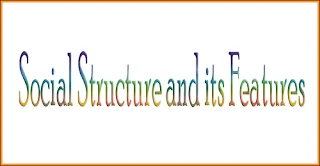 |
| Social Structure and its Features |
Thursday, 15 December 2022
 |
| The Achievements of Louis XIV |




